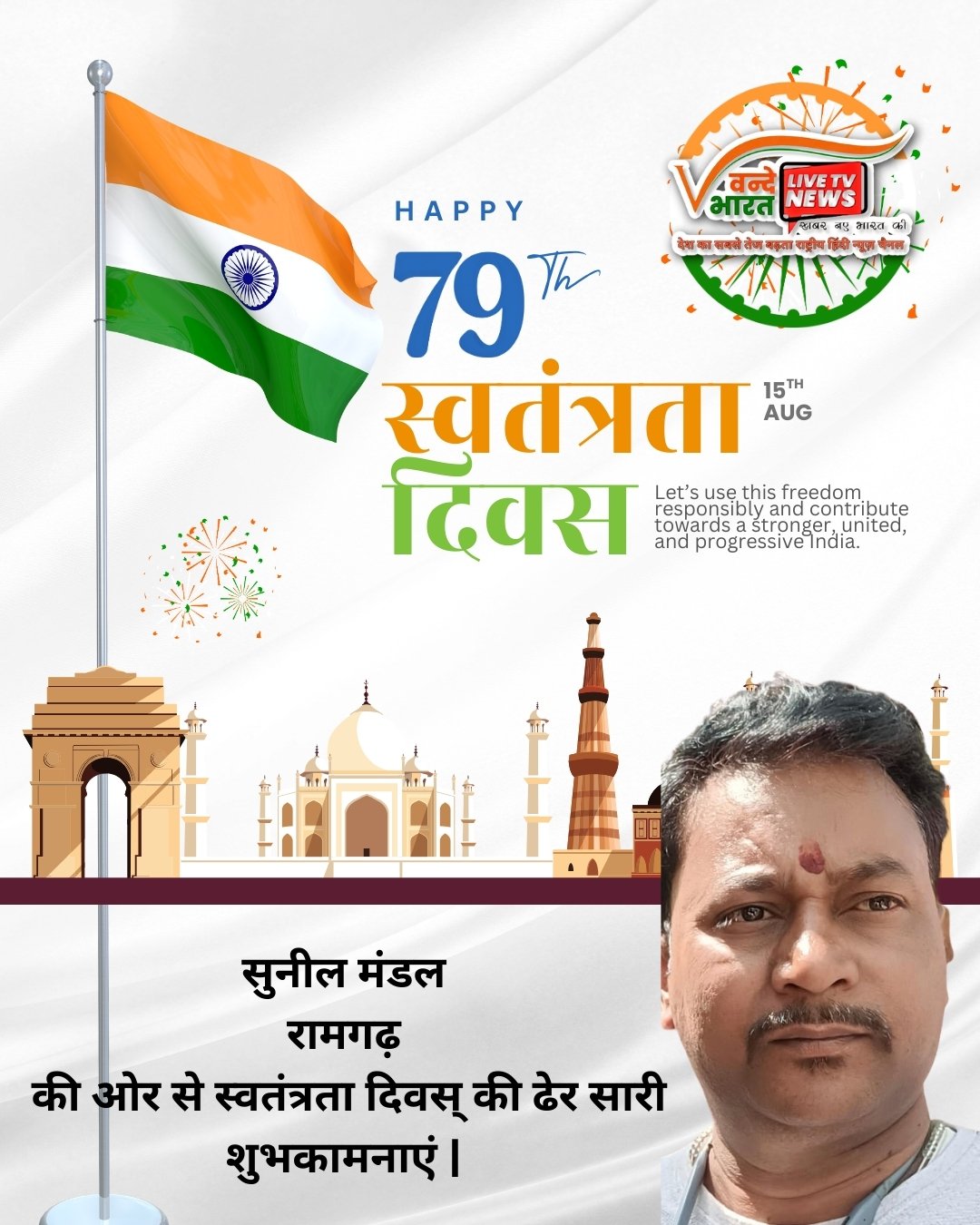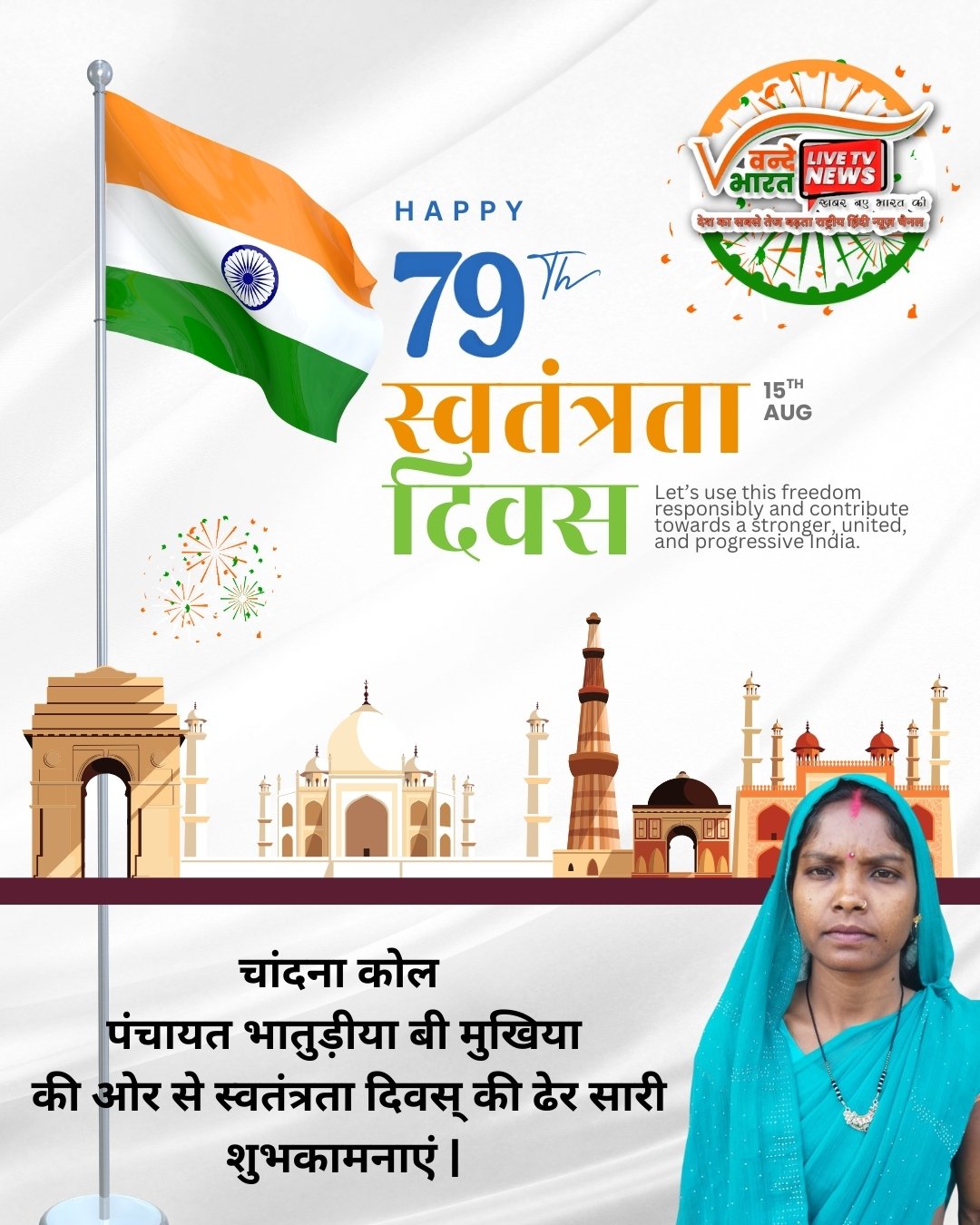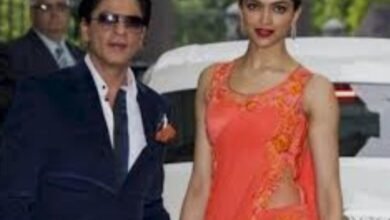प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली
पत्रकारिता पर डीपीडीपी क़ानून के प्रभाव: प्रेस संगठनों ने मंत्रालय को 35 सवाल भेजे
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी कानून में पत्रकारों को छूट, डेटा सुरक्षा, आरटीआई संशोधन, स्रोत की सुरक्षा, सहमति, और न्यूज़रूम स्वतंत्रता समेत 35 सवाल मंत्रालय को भेजे हैं. यह सवाल क़ानून के जनहित पत्रकारिता पर संभावित असर और सुरक्षा उपायों पर केंद्रित हैं.
नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) और इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स (आईडब्लूपीसी) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी (डीपीडीपी) कानून को लेकर अपनी चिंताओं के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल 35 सवाल सौंपे हैं.
ये सवाल एक ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (एफएक्यू- FAQ) की सूची का हिस्सा हैं, जिसे मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने 28 जुलाई को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, आईडब्लूपीसी, डिजीपब और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से हुई बैठक के दौरान मांगा था.
यह बैठक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहल पर बुलाई गई थी. प्रेस क्लब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाक़ात का समय मांगा था और उन्हें – प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के प्रमुख महानिदेशक के माध्यम से – एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा था. इस ज्ञापन पर देशभर की 21 चुनी हुई प्रेस संस्थाओं और एक हज़ार से अधिक पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए थे.
ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई थी कि कानून में पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई है. लेकिन मंत्री से मुलाक़ात का समय देने के बजाय मंत्रालय के सचिव ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की और ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की.
इसके बाद प्रेस क्लब और आईडब्लूपीसी ने अपने सदस्यों की बैठक कर सुझाव जुटाए और 35 सवालों की एक सूची तैयार की, ताकि प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जा सके. उनका कहना है कि यह कानून पत्रकारों के काम करने के अधिकार (अनुच्छेद 19 के तहत संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार) का उल्लंघन कर सकता है.
23 अगस्त को ये सवाल मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पीआईबी के प्रधान महानिदेशक धीरेंद्र ओझा को सौंपे गए, ताकि उनके माध्यम से सचिव तक पहुंच सके.
कृष्णन को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि एफएक्यू की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, वे सिर्फ मंत्रियों की ओर से स्पष्टीकरण होते हैं. इसलिए प्रेस संस्थाओं और पत्रकारों की मूल मांग वही बनी रहती है कि कानून में संशोधन कर साफ तौर पर यह पंक्ति जोड़ी जाए कि – ‘पत्रकारीय कार्य को छूट है.’
नीचे वो सवाल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भेजे गए थे:
1. 2018, 2019 और 2021 में बने डेटा प्रोटेक्शन बिल के संस्करणों में पत्रकारिता के लिए छूट दी गई थी. जस्टिस श्रीकृष्ण समिति की डेटा प्रोटेक्शन रिपोर्ट (2018) और 2012 में जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता वाली प्राइवेसी विशेषज्ञ समिति ने भी पत्रकारिता के लिए छूट देने की सिफारिश की थी. तो आखिरकार अगस्त 2023 में बने डीपीडीपी बिल में पत्रकारिता के लिए यह छूट क्यों हटा दी गई?
2. अगर मंत्रालय की राय में पत्रकारिता के काम पर यह कानून लागू नहीं होता इसलिए कोई अलग छूट देने की जरूरत नहीं है, तो डीपीडीपी एक्ट, 2023 की कौन-कौन सी धाराएं हैं जो उन लोगों और संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करती हैं और उन्हें डेटा फिड्यूशियरी की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हैं, जब वे पत्रकारिता के उद्देश्य से व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर रहे हों? कृपया ऐसी धाराओं की सूची दें और समझाएं कि ये पत्रकारिता को कैसे सुरक्षित रखती हैं.
3. 2005 में आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद, कानून के तहत प्राप्त जानकारी पत्रकारों और मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जनहित में पत्रकारिता के काम आरटीआई से मिली जानकारी पर आधारित हैं. डीपीडीपी एक्ट के जरिए आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) में संशोधन करके जानकारी के खुलासे से छूट का दायरा बढ़ाने का कारण क्या था?
4. अगर मंत्रालय की राय में आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी तक पहुंच का अधिकार डीपीडीपी एक्ट के जरिए धारा 8(1)(j) में बदलाव के बावजूद वही रहता है क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(2) मौजूद है, तो फिर आरटीआई एक्ट में संशोधन क्यों किया गया?
5. धारा 44(3) ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) को बदल दिया है, जिससे अब सभी व्यक्तिगत डेटा को खुलासे से छूट दी गई है, और पहले की तरह ‘जनहित में खुलासा’ की छूट अब नहीं है. ऐसे में मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि भ्रष्टाचार से जुड़े रिकॉर्ड तक पत्रकारों की पहुंच कमजोर न हो?
6. पत्रकारिता के काम में कभी-कभी दस्तावेज़ों को साझा और संग्रहित करना पड़ता है, जिनमें व्यक्तिगत जानकारी भी होती है, और ये दस्तावेज़ कई बार राष्ट्रीय सीमाओं और अलग-अलग ज्यूरिस्डिक्शन्स में भेजे जाते हैं. कभी-कभी ऐसे दस्तावेज़ ह्विसिलब्लोअर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए उनकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों की जरूरत होती है, जैसे कि इस जानकारी को सुरक्षित सर्वर पर स्टोर और प्रोसेस करना, जो भारत के बाहर स्थित हो सकते हैं. डीपीडीपी एक्ट की विभिन्न धाराएं, जैसे धारा 16, व्यक्तिगत डेटा के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती हैं. ऐसे में पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर जानकारी का प्रोसेसिंग और संग्रह कैसे सुरक्षित रखा जाएगा?
7. क्या डीपीडीपी एक्ट, 2023 की धारा 2 में दी गई ‘ऑटोमेटेड’, ‘डेटा फिड्यूशियरी’, ‘डेटा प्रिंसिपल’ और ‘डेटा प्रोसेसर’ की परिभाषाएं पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों और मीडिया संस्थाओं पर लागू होती हैं? हां या नहीं?
8. अगर जवाब ‘नहीं’ है, तो एक्ट में पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों और मीडिया संस्थाओं के लिए धारा 17 में छूट को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा गया?
9. अगर जवाब ‘हां’ है, तो पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों और मीडिया संस्थाओं पर ‘डेटा फिड्यूशियरी’, ‘डेटा प्रोसेसर’, ‘व्यक्तिगत डेटा’ और ‘डेटा प्रिंसिपल’ की परिभाषाओं से कौन-कौन सी छूट लागू होगी?
10. ड्राफ्ट नियम 8 कहता है कि व्यक्तिगत डेटा तीन साल बाद डिलीट कर दिया जाएगा और इससे पहले 48 घंटे की चेतावनी दी जाएगी. समाचार संग्रह का ऐतिहासिक महत्व देखते हुए, क्या मंत्रालय यह पुष्टि करेगा कि पत्रकारिता के संग्रह ‘अनुसंधान, अभिलेखागार और सांख्यिकीय उद्देश्यों’ के अंतर्गत आते हैं जैसा कि धारा 17 में छूट दी गई है?
11. ड्राफ्ट नियम 15 के अनुसार, लंबे समय तक न उपयोग किए गए डेटा को डिलीट करने का कारण बन जाता है. क्या पत्रकारिता के काम में स्रोत से संबंधित फ़ाइलें, जो केवल जनहित के फॉलो-अप के लिए रखी गई हैं, अनिवार्य रूप से डिलीट शेड्यूल में आएंगी या इन्हें सुरक्षा दी जाएगी?
12. क्या मंत्रालय धारा 40 के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके न्यूज़ गेदरिंग (खबर एकत्र करने) के लिए छूट देगा, या पत्रकारों को केवल धारा 7 में वर्णित संकीर्ण ‘कुछ वैध उपयोग’ पर भरोसा करना होगा?
13. क्या पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से पूर्व सहमति लेनी होगी, जिनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पहचान विवरण प्रेस रिपोर्ट में शामिल हैं?
14. रिपोर्टिंग में अक्सर नाम, उम्र, लिंग, स्थान, पेशा, जाति, वर्ग, आय जैसी जानकारियां चाहिए होती हैं ताकि कहानी की पुष्टि हो सके. इन जानकारियों में से अधिकांश ‘व्यक्तिगत डेटा’ की परिभाषा में आते हैं. अगर इन जानकारियों को हटाना पड़े तो खबर अधूरी और अस्पष्ट हो जाएंगी. ऐसी स्थिति में, एक्ट की कौन-कौन सी धाराएं पत्रकारिता के काम में इन जानकारियों को प्रकाशित करने की छूट देती हैं?
15. पल-पल बदल रही खबरों जैसे दंगा, आतंकवादी हमला, प्राकृतिक आपदा आदि की रिपोर्टिंग में, क्या पत्रकार को कहानी रिपोर्ट करने से पहले धारा 5 और 6 के तहत सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी?
16. ड्राफ्ट नियम 3 कहता है कि डेटा फिड्यूशियरी की सूचना ‘साफ और सरल भाषा’ में पहले दी जाए. लाइव रिपोर्टिंग, साक्षात्कार, गुप्त रिपोर्टिंग आदि कैसे इसे पूरा कर सकते हैं? क्या मंत्रालय स्पष्ट करेगा कि जनहित में पत्रकारिता के लिए पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं है?
17. किसी मंत्री, नौकरशाह या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले में, क्या पत्रकार या मीडिया संगठन को आरोपी से ‘सूचित सहमति’ लेनी होगी, जिस फॉर्म और प्रारूप में जानकारी एकत्र की गई है, उससे पहले कि वे लेख प्रकाशित करें?
18. कस्टोडियल टॉर्चर या मौत के मामले में, क्या पत्रकार या मीडिया संगठन को आरोपी पुलिस अधिकारी से धारा 6 के तहत सहमति लेनी होगी, इससे पहले कि वह नाम, पोस्टिंग जगह या घटना की जानकारी प्रकाशित करे?
19. धारा 7 कहती है कि ‘डेटा प्रिंसिपल’ का व्यक्तिगत डेटा केवल ‘निर्दिष्ट उद्देश्य’ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे मामलों में पत्रकारों और मीडिया संस्थाओं के लिए ये परिस्थितियां कैसे लागू होंगी?
परिस्थिति-1
मान लीजिए कि पत्रकारिता में शामिल एक व्यक्ति एक रिपोर्ट पर काम कर रहा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को राशन कार्ड न मिलने का मामला है, जो कि उनके आधार डेटा के मेल न खाने के कारण हुआ है. इस दौरान वह प्रभावित लोगों का व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करता है, जैसे नाम, उम्र, और स्थान, ताकि समस्या की व्यापकता को पहचाना जा सके. इस स्थिति से कुछ सवाल उठते हैं:
i) क्या पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति को इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करने और इसे किसी लेख में तालिका के रूप में इस्तेमाल करके सार्वजनिक हित में प्रणालीगत समस्या को उजागर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से ‘सूचित सहमति’ लेनी होगी?
ii) चूंकि यह मामला आधार प्रणाली में अंतर्निहित दोषों से जुड़ा है, क्या पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कि आधार आधारित राशन कार्ड के कारण लोगों को भोजन से वंचित किया जा रहा है, UIDAI के संबंधित अधिकारी से ‘सूचित सहमति’ लेनी होगी?
परिस्थिति-2
मान लीजिए, कुछ महीनों बाद यह सामने आता है कि उसी क्षेत्र में भोजन की पहुंच न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई है, और पहले इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया जा रहा है कि ये मौतें आधार डेटा की समस्याओं से जुड़ी हैं.
क्या इस स्थिति में पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति या मीडिया संगठन को फिर से सहमति लेनी होगी?
20. ड्राफ्ट नियम 10(1) के अनुसार, आउटलेट्स को बच्चे के डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की सहमति लेनी होगी. पत्रकारिता में लगे लोग या मीडिया संगठन ऐसे मामलों में, जहं नाबालिगों (18 वर्ष और उससे कम) से जुड़े मुद्दों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग करनी हो, इस नियम का उल्लंघन किए बिना इसे कैसे कवर कर सकते हैं?
21. धारा 10 के अनुसार, केंद्र सरकार को किसी भी डेटा फिड्यूशियरी को ‘सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी’ के रूप में नोटिफाई करने का विवेकाधिकार है. क्या इसका मतलब यह है कि पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति या मीडिया संगठन, जो बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा संभालते हैं, उन्हें भी ‘सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी’ के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है? हां या नहीं?
22. अगर उत्तर नहीं है, तो एक्ट की कौन सी धारा के तहत छूट दी जाएगी?
23. धारा 10 के तहत किसी डेटा फिड्यूशियरी को ‘चुनावी लोकतंत्र, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा’ के जोखिम के आधार पर नोटिफाई किया जा सकता है. बड़े या महत्वपूर्ण मीडिया हाउसों को केवल जांची-परखी कहानियां प्रकाशित करने के लिए ‘सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी’ अनुपालन में कैसे नहीं डाला जाएगा, इसके लिए कौन-कौन से उद्देश्यपूर्ण मानदंड लागू होंगे?
24. ड्राफ्ट नियम 22(1) कहता है कि अगर सरकार किसी डेटा फिड्यूशियरी (डेटा संभालने वाले व्यक्ति या संगठन) से कोई जानकारी मांगती है, तो वह आदेश दे सकती है कि डेटा फिड्यूशियरी यह न बताए कि सरकार ने यह अनुरोध किया है. जबकि पत्रकारों को यह अधिकार है कि वे सरकार की कार्रवाई पर रिपोर्ट करें. ऐसे में मंत्रालय यह बताए कि कैसे गुप्त आदेशों और पत्रकारों के रिपोर्टिंग के अधिकार को संतुलित किया जाएगा, ताकि पत्रकार काम कर सकें और जनता को जानकारी मिलती रहे, लेकिन सुरक्षा या गोपनीयता भी बनी रहे.
25. धारा 28 की उप-धारा (7) के क्लॉज़ (c) और धारा 36 डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार देती हैं कि वे ‘किसी भी डेटा, किताब, दस्तावेज़, रजिस्टर, खाता-बही या अन्य कोई दस्तावेज़’ मांग सकते हैं. अब, खोज़ी पत्रकारिता काफी हद तक ‘स्रोत-आधारित जानकारी’ या ह्विसिलब्लोअर द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करती है. इतने व्यापक अधिकार होने के कारण, बोर्ड पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति या मीडिया संगठन से ‘स्रोत’ का खुलासा करने को भी कह सकता है. ऐसे मामले में पत्रकार और मीडिया संगठनों को स्रोत की सुरक्षा के लिए एक्ट के तहत कौन-कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं?
26. ड्राफ्ट नियम 6(g) कहता है कि ‘सुरक्षा उपायों का सही पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक कदम उठाए जाएं’ और इसे बोर्ड लागू कर सकता है. सवाल यह है कि ऐसे निरीक्षणों की सीमा क्या होगी, ताकि ये न्यूज़रूम की तलाशी में न बदलें और संपादकीय स्वतंत्रता पर असर न पड़े?
27. ड्राफ्ट नियम 7 के अनुसार, डेटा फिड्यूशियरी को डेटा लीक होने पर हर प्रभावित व्यक्ति को सूचित करना होगा. अगर किसी कंपनी, पीएसयू, सरकारी विभाग आदि में ह्विसिलब्लोअर गलत काम का खुलासा करता है, तो क्या पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति या न्यूज़रूम को जांच में शामिल अधिकारियों को सूचित करना होगा, ऐसे में उसका स्रोत उजागर हो सकता है?
28. ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, बोर्ड कंसेंट मैनेजर के पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है और जानकारी जाहिर करने के लिए बाध्य कर सकता है. अगर किसी मीडिया द्वारा चलाए जा रहे कंसेंट टूल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो क्या अपील का विकल्प होगा, और चल रहे सब्सक्रिप्शन कैसे बनाए रखे जाएंगे?
29. ड्राफ्ट नियम 6 में एन्क्रिप्शन, विस्तृत लॉगिंग और एक साल के लॉग रख-रखाव की आवश्यकता है. छोटे, स्वतंत्र आउटलेट्स के लिए, जिनके पास एंटरप्राइज-ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है, क्या वित्तीय या तकनीकी सहायता दी जाएगी?
30. धारा 7(b) के अनुसार, सरकार लोगों को मिलने वाले लाभ या सब्सिडी देने के लिए नागरिकों का डेटा इस्तेमाल कर सकती है. नियम 5 कहता है कि इसके लिए लोगों की अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बस कुछ न्यूनतम सुरक्षा मानक पूरे करने होंगे. ऐसे में इस डेटा का इस्तेमाल उस पत्रकार की पहचान करने और उससे बदला लेने के लिए की जा सकती है, जो सरकार से सवाल पूछता है. सवाल यह है कि कानून में कौन से सुरक्षा उपाय होंगे, ताकि यह डेटा सिर्फ सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल हो, और पत्रकारों या मीडिया के खिलाफ गलत तरीके से न इस्तेमाल किया जाए.
31. बार-बार नियमों का पालन न करने पर, आईटी एक्ट और डीपीडीपी की धारा 37 के तहत डेटा सुरक्षा कारणों से किसी न्यूज़ साइट को ब्लॉक किया जा सकता है. क्या मंत्रालय यह वचन देगा कि किसी भी न्यूज़ साइट को बंद करने से पहले न्यायालय की अनुमति ली जाएगी?
32. ब्लॉकिंग कार्रवाई शुरू करने से पहले नियम न पालन करने की कितनी बार की सीमा तय है?
33. जब दंड तय किए जा रहे हों, धारा 33 बोर्ड को यह निर्देश देती है कि ‘उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि’ पर विचार किया जाए. चूंकि ईमानदार जनहित पत्रकारिता में लीक डेटा शामिल हो सकता है, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जुर्माने की राशि छोटे न्यूज़रूम और पत्रकारों में डर पैदा न करे?
34. मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि डीपीडीपी के तहत सहमति और नोटिस देने के नियम और प्रेस एक्ट व वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट में मिले कानूनी अधिकार एक-दूसरे के साथ टकराएं नहीं और सहज रूप से लागू हों?
35. चूंकि केंद्र सरकार को आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जानकारी या सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार दिया गया है, फिर धारा 37(1)(b) को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, जो डीपीडीपी के तहत एक अलग ब्लॉकिंग व्यवस्था बनाता है और सरकार को और अधिक अधिकार देता है कि वह ब्लॉकिंग के निर्देश जारी कर सके?
RNI:- MPBIL/25/A1465
Devashish Tokekar
Vande bharat live tv news,nagpur
Editor
Indian Council of press,Nagpur
Journalist
Contact no.9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015